जानिये क्या है भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार
!
दोस्तों, संविधान के भाग III में परिभाषित किये गए 12 से
35 तक तथा मुख्य रुप से 7 मौलिक अधिकारोँ को बताया गया है,
परन्तु 44 वेँ संविधान संशोधन
के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधायी अधिकार में बदल दिया गया है , जिससे
मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई हैं । मौलिक अधिकारोँ के बदलाव के संबंध मेँ राज्य
की विधान सभाओं को कोई विधि बनाने का अधिकार नहीँ दिया गया है, केवल संसद को यह अधिकार
प्राप्त है।
आज हम
आपको इस आर्टिकल के द्वारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से आपको अवगत कराने जा
रहे है , जिससे आपको अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त होगी | आप इस जानकारी
के माध्यम से अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने से बच सकेंगे | भारत के संविधान के अनुसार
भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार दिए गए है |
भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार-
समता
या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18) |
स्वतंत्रता
का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22) |
शोषण
के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24) |
धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28) |
संस्कृति
और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30) |
संवैधानिक
उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) |
समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद
18)-
अनुच्छेद
14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता तथा विधि को समान संरक्षण प्रदान किया गया है
|
अनुच्छेद
15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
किया जाने का अधिकार दिया गया है |
अनुच्छेद
16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जिसके तहत राज्य के अधीन किसी
पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए
जाएंगे |
अनुच्छेद
17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु इसे दंडनीय अपराध माना जायेगा |
अनुच्छेद
18 के अंतर्गत उपाधियोँ का अंत किया गया है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के
अतिरिक्त और कोई उपाधि राज्य द्वारा तथा अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के
नहीँ प्राप्त कर सकता है |
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)-
वाक्,
स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार |
शांतिपूर्ण
और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का अधिकार |
संगम
या संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार |
भारत
के राज्य क्षेत्र मेँ सर्वत्र आबाध संचरण करने का अधिकार |
भारत
के राज्य क्षेत्र मेँ किसी भाग मेँ निवास करना या बस जाने का अधिकार |
कोई
वृति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार |
इस अधिकार
के अंतर्गत कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध,
सार्वजनिक व्यवस्था, शालीलनता और नैतिकता के अधीन प्रदान किये गए हैं।
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से
24)-
अनुच्छेद
23 के तहत मानव के व्यापार और बलात्श्रम पर रोक, मानव का दुर्व्यापार और बेगार प्रथा
उल्लंघन करने पर अपराधी माना जायेगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा |
अनुच्छेद
24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान मेँ काम करने के
लिए नियुक्ति नहीँ किया जाएगा।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से
28)-
अनुच्छेद
25 के अंतर्गत अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
की लिए स्वतंत्र होगा |
अनुच्छेद
26 के अंतर्गत धार्मिक कार्योँ के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार |
अनुच्छेद
27 के अंतर्गत धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान के बारे मेँ स्वतंत्रता का
अधिकार दिया गया है |
अनुच्छेद
28 के अंतर्गत सभी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित
होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है |
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद
29 से 30)-
भारत
के राज्य क्षेत्र के निवासी नागरिकोँ के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी, लिपि, संस्कृति
या भाषा है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है |
धर्म
या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग को को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित
करने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार है |
किसी
भी नागरिक को केवल जाति, भाषा, मूलवंश या धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीँ किया
जाने का अधिकार |
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32 से
35)-
अनुच्छेद
32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु समुचित कार्यवाहियों के माध्यम
से उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है | जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय
को पांच तरह के रिट निकालने की शक्तियां दी गई है | जो इस प्रकार है -
बंदी प्रत्यक्षीकरण-
यह रिट
तब जारी की जाती है, जब किसी को अवैधानिक रुप से दोषी न हो। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत
स्वतंत्रता का संरक्षण करना होता है। अवैधानिक रूप से दोषी न पाया जाने वाला व्यक्ति
न्यायालय द्वारा मुक्त किया जा सकता है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती
|
परमादेश-
यह तब
लागू होता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है. इस
प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने हेतु आदेश
दिया जाता है |
Read Also: क्या है देश के राष्ट्पति
के अधिकार - जानिये
प्रतिषेध लेख-
इसका
प्रयोग सिर्फ न्यायिक और अल्प न्यायिक प्राधिकारिओं के विरुद्ध किया जा सकता है | यह
आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्द्ध
न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेशित किया जाता है कि इस मामले में अपने
यहां कार्यवाही न करें | यह क्षेत्र उनके मामलों के अंतर्गत नहीं है |
उत्प्रेषण-
इसके
अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों
के न्याय निर्णयन के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें |
अधिकार पृच्छा लेख-
इसका
प्रयोग केवल लोक अधिकारी के विरोध मेँ किया जाता है तथा इसके अंतर्गत सुनिश्चित करते
है कि लोक अधिकारी के पद पर आसीन व्यक्ति, उस पद की अर्हता को पूरा करता है या नहीं
| इसका प्रयोग याचिका के माध्यम से किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है |
दोस्तों,
उपरोक्त दी गई जानकारी के माध्यम से अब आपको अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी प्राप्त
करने में अवश्य मदद मिलेगी |यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न या विचार आ रहा है तो
कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछें | आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया की हम प्रतीक्षा
कर रहें है |
यदि
आप डेली करंट अफेयर , आर्टिकल , नौकरी सम्बन्धी तथा करियर से संबंधित प्राप्त करना
चाहते है तो हमारें sarkarinaukricareer.in पोर्टल पर लॉगिन करें | यदि आपको यह आर्टिकल
पसंद आया तो हमारे facebook पेज को जरूर Like करें |
Advertisement

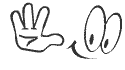

No comments:
Post a Comment
If you have any query, Write in Comment Box